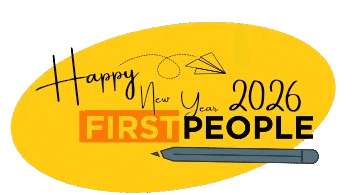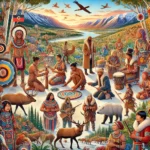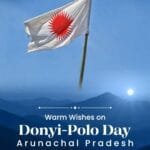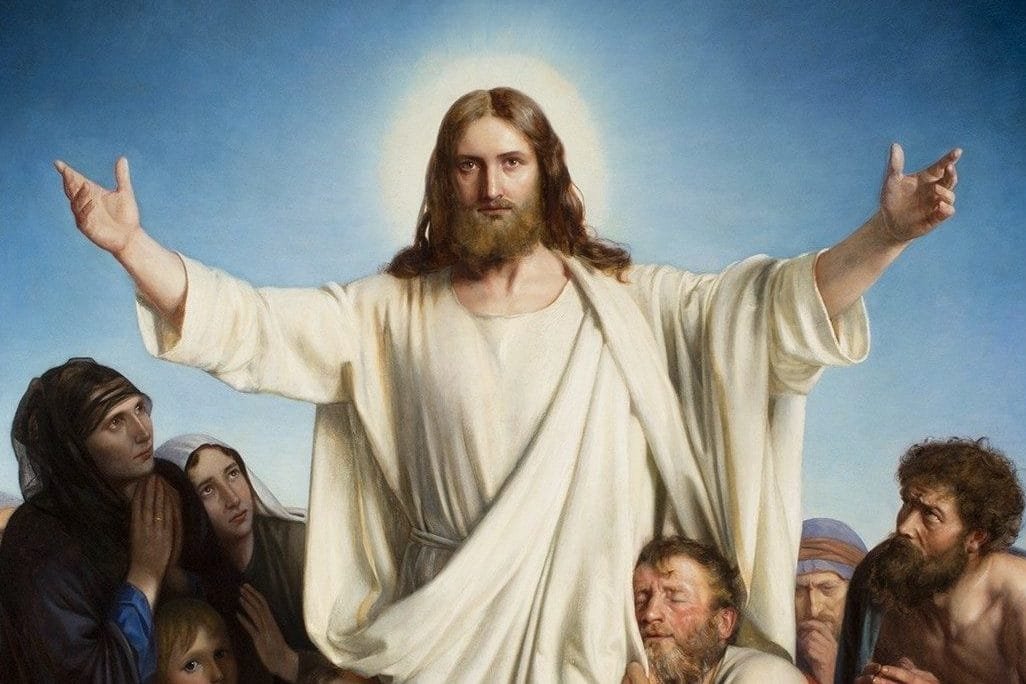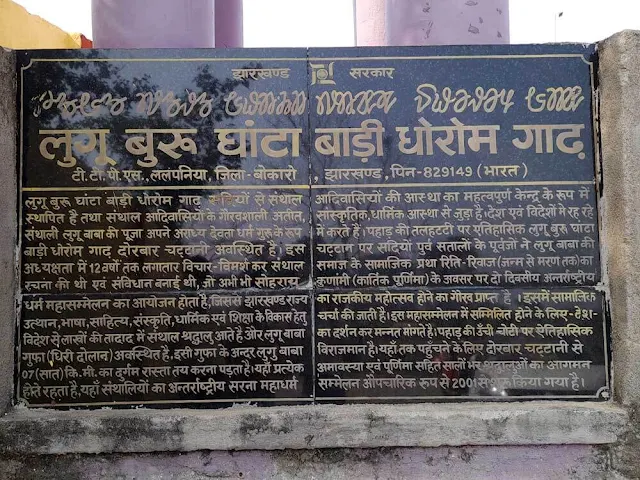गणेश माँझी
गोम्हा पूनी यानि सावन के महीने का आखिरी और पूर्णिमा का दिन. गोमहा पूनी तक रोपा-रोपने के बाद फसल खेतों में लगभग बढ़ने वाले स्थिति में होते हैं, हालाँकि अब धीरे-धीरे ये प्रक्रिया धीमी हो चुकी है, शायद जलवायु परिवर्तन, समय से बारिश का न होना एक वजह हो सकता है. बचपन से ही देखा है गोमहा पूनी के दिन गाँव घर के चारों ओर साफ़-सफाई किया जाता है. साफ़-सफ़ाई का गांव में अलग ही उत्साह होता है और अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन कुछ अलग ही महसूस होता है.
फसल जब लगभग लहलहाने लगते हैं, फसलों में कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंग आक्रमण शुरू कर देते हैं. इस समस्या का आदिवासियों के बीच प्राकृतिक समाधान रहा है. गोमहा पूनी के दिन कुछ लड़के/ पुरुष सुबह ही जंगल जाकर केऊंद (केन्दु) के बहुत सारे छोटे पेड़ (गांव में गहरे खेतों की संख्या अनुसार) को काट कर लाते हैं, साथ में महादेव जट्ट की लत्ता, भेलवा (सोसो) की पत्तियां, और चिरचिट्ठी का पौधा भी ले आते हैं. केऊंद (केन्दु) के छोटे पेड़ के एक सिरा को चीड़कर इन सारे पौधों और पत्तियों को लगाया जाता है.
तत्पश्चात इन सारे पौधे को एक जगह पर रखकर पूजा किया जाता है, कहीं-कहीं पर मुर्गे की बलि देकर भोज्य पदार्थ के रूप में पूर्वजों के साथ साझा किया जाता है, ताकि वे सुख-दुःख का हिस्सा बने रहें और पौधों की रखवाली में मदद भी करते रहें. पूजा के पश्चात, केऊंद (केन्दु) के इस छोटे पेड़ को गहरे वाले खेतों के बीच में गाड़ दिया जाता है. अगर आपके मन में सवाल है कि केऊंद (केन्दु) के छोटे पेड़ों को ही क्यों काटना है, इसका जवाब ये है की इसके पौधे गाँवों में बहुतायत में होते हैं.
काफी बार खेती योग्य टांड़ के निर्माण में इन छोटे पेड़ों और पौधों को साफ़ किया जाता है. केऊंद (केन्दु) के पत्ते का ही इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है. तेन्दु/केऊंद (केन्दु) के पत्ते का व्यवसाय बहुत बड़ा है.
महादेव जट्ट की लत्ता, भेलवा (सोसो) की पत्तियां, और चिरचिट्ठी का पौधा इन सारे पौधों और लताओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभ अभी भी खोज का विषय है लेकिन फसलों को बचाने का एक जरिया जरूर है. एक प्रत्यक्ष फ़ायदा ये होता है की बीच में गाड़े गए इस छोटे से पेड़ में पक्षियां उड़ कर आती हैं, खेत के बीच वाले खूंटे में बैठती हैं, धान के पौधों को हानि पहुँचाने वाले कीड़े-मकोड़े और कीट-पतंगों का सफाया करतीं हैं. केऊंद (केन्दु) के इस छोटे पेड़ को लेकर खेतों में गाड़ने तक की पूरी प्रक्रिया को ‘भाख खूंटा’ गाड़ना कहते हैं.
गोमहा और भाख़ खूंटा का दर्शन और फसल से जुड़ी समस्याओं का प्राकृतिक समाधान है. आदिवासी समुदायों के ग्रामीण पृष्ठभूमि में महादेव जट्ट को रानू (हँड़िया बनाने के लिए तैयार की गयी सफ़ेद सी गोली) और पेशाब के अत्यधिक पीलापन होने पर दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. चिरचिठी पौधे का इस्तेमाल भी दवाई के रूप में होता रहा है, हालाँकि इन सारे पौधों का वैज्ञानिक अनुसन्धान से सत्यता की जाँच जरुरी है.
काफी सारे आदिवासी और गैर- आदिवासी समुदायों के खेतों में भाख खूंटा देखने को मिलेगा. झारखण्ड के काफी सारे समुदायों में लगभग यही प्रक्रिया ‘करम’ त्यौहार के दूसरे दिन भी किया जाता है. करम त्यौहार भाद्रपद महीने की एकादशी को मनाई जाती है.
दिन में, मवेशियों को खेतों, जंगलों में चराने, घुमाने के बाद जब वापस लाया जाता है तो सोहराई में जिस प्रक्रिया से दाना (कोंहड़ा, उड़द और कुछ अन्य अनाजों को पकाकर तैयार किया हुआ) खिलाया जाता है उसी प्रक्रिया से गोम्हा पूनी के दिन भी महुआ के साथ अन्य अनाजों को मिलाकर खिलाया जाता है. खिलाने से पहले मवेशियों के पैर और सींग धोये जाते हैं और तेल भी लगाए जाते हैं.
पालतू पशुओं (मवेशियों) के साथ सौहार्दता और सहजीवन का ये अलग ही नमूना है जो अन्य मानव जातियों में शायद ही देखने को मिलेगा.
संयोग से गोमहा पूनी के दिन ही हिन्दू समाज/ सनातन समाज रक्षा बंधन मनाता है. ऐतिहासिक रूप से रक्षा बंधन की शुरुवात कैसे हुई थी हम इसपर नहीं जाएंगे लेकिन अबतक की जानकारी के मुताबिक, बहन (एक लड़की) अपने भाई को ही राखी बांधे इसका पुख्ता साक्ष्य नहीं है. इतना जरूर है एक लड़की/ महिला अक्सर एक पुरुष को ही राखी बांधती है, शायद इस आशा में की वो पुरुष हर परिस्थिति में उस महिला की रक्षा करेगा.
मतलब ऐतिहासिक रूप से महिला को पुरुषों से कमजोर मान लिया गया है और ऐसा लगता है महिला भी सहमत है अन्यथा ऐसे त्योहार के 21वीं सदी में भी मनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है. खैर, गोमहा पूनी के दिन ही दूसरी बेला में गोसाईं/ पंडित आता था अपने साथ लाल-धागा लेकर और घर-घर घूमकर सबको तथाकथित रक्षा-सूत्र (लाल धागा) बांधता था और अपने साथ ढेर सारा धान बटोर के ले जाता था. फिर धीरे-धीरे लोग बाजार से प्रभावित होकर राखी खरीद कर लाने लगे और अपने भाइयों को बाँधने लगे. अब आदिवासी लोग भी गोमहा पूनी कम और रक्षा बंधन ज्यादा मनाने लगे हैं.
गोमहा पूनी सावन महीने के अंतिम दिन में मनाये जाने का ये भी मतलब नहीं है कि आदिवासी समुदाय बहंगी में या लोटे में या घड़े में पानी लेकर शिवलिंग पर जल चढाने जाते हैं। प्रभाववश कुछ आदिवासियों को करते हुए आप जरूर देख सकते हैं लेकिन वो बृहत् आदिवासी समाज की सोच और मान्यता नहीं है. मतलब पंडित का और बाजार का अतिक्रमण, आदिवासी त्योहारों, मान्यताओं का सांस्कृतिकरण, और आदिवासी समाज के इतिहास का मिटान का स्वरुप गोमहा पर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है.
बाजार और हिन्दुकरण का प्रभाव के बाद दूसरा प्रभाव भी आपको यत्र-तत्र देखने को मिल जायेगा. जैसे: ईसाई धर्म अपनाने के बाद कुछ आदिवासी लोगों ने भाख़ खूंटा की जगह क्रॉस लगाते हैं. भाख खूंटा गाड़ने की मान्यता प्रत्यक्ष रूप से क्रॉस द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है. लेकिन इस विस्थापन का दर्द कहीं नहीं होता है क्योंकि विस्थापन के पहले दिमाग में विस्थापन की महिमा बैठा दी गयी है. ईश्वर से प्रार्थना या पूर्वजों से आग्रह, आराधना जैसी भी हो उद्देश्य वही है लेकिन प्रतीकों को छोड़ना और बदल देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है क्योंकि इससे त्योहारों, इनकी मान्यताओं और परम्पराओं का क्षय होता है जो धीरे-धीरे आपके आदिवासी और आदिवासियत को लीलने का काम कर रहा है. आदिवासी समाज में नए ईश्वर और धर्म के आगमन से सामुदायिक जीवन, इनके ऐतिहासिक चिन्हों, मान्यताओं और तथ्यों पर भी अतिक्रमण और मिटान स्पष्ट देखा जा सकता है. सांस्कृतिकरण अब काफी पुराना हो चुका है, अब इसकी जगह धीरे-धीरे धार्मिक साम्राज्यवाद ने ले लिया है.