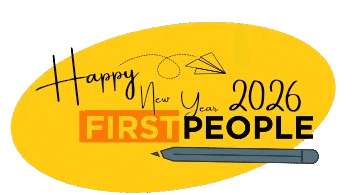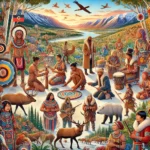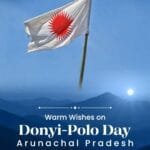*”भारत के आदिवासी समुदाय सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति के सच्चे संरक्षक माने जाते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ की धरती पर सरना धर्म ‘जाहेरथान’ और ‘मरांग बुरू’ की पूजा से जीवन को दिशा देता है। अरुणाचल की पहाड़ियों में डोनी-पोलो – यानी सूरज और चाँद – लोगों के जीवन का प्रकाश और समय का चक्र बनते हैं। मेघालय के पहाड़ों में नियमत्रे (Niamtre) धर्म, प्रकृति और पूर्वजों के प्रति आस्था को जोड़ता है। छत्तीसगढ़ और आंध्र की बस्तियों में कोया पुनेम आदिवासी समाज को अपनी जड़ों और अपनी धरती से जोड़े रखता है। मणिपुर की घाटियों में सनामाही धर्म – घर-घर में पूजे जाने वाले देवता, जिनकी उपस्थिति हर परंपरा में दिखती है।
यही नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों में गोंडी, भील, हो, खासी, मिज़ो, नागा, मुण्डा, साओरा, और संथाल – सबकी अपनी अलग आस्थाएं, अपने पर्व, अपने देवता और अपनी अनूठी परंपराएं हैं।
ये धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि धरती, जंगल, जल और पूर्वजों से रिश्ता जोड़ने का तरीका हैं। लेकिन सवाल है—क्या यह विरासत आज सुरक्षित है? क्यों आज लाखों आदिवासी यह महसूस करते हैं कि उनकी अपनी परंपराएं धीरे-धीरे मिटाई जा रही हैं? और क्या इसके पीछे किसी बड़ी रणनीति का हाथ है? इसी सवाल से जुड़ती है चर्च और मिशनरी गतिविधियों की वह कहानी, जिसे समझना आज ज़रूरी है।”
चर्च और धर्मांतरण का प्रवेश
*”आज एक गंभीर चर्चा जरूरी है—आदिवासी समाज और चर्च के रिश्ते की। चर्च और मिशनरी संगठन हमेशा दावा करते हैं कि वे किसी का धर्मांतरण नहीं कराते, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा का काम करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है?
Pew Research Center के मुताबिक, भारत में ईसाई आबादी 2.3% है। लेकिन इसी रिपोर्ट और Oxford Research के अध्ययन बताते हैं कि—ईसाई आबादी में एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों और दलितों का है। कई जगहों पर अनुमान है कि भारत के ईसाई समुदाय में 30 से 40 फीसदी लोग आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। और जब इसमें दलित ईसाई शामिल कर दिए जाएं, तो यह आंकड़ा 60 फीसदी तक पहुँच जाता है।*
Pew Research Center (2021):
भारतीय ईसाइयों में से 24% Scheduled Tribes (ST) से आते हैं, और 33% Scheduled Castes (SC) हैं .
→ मतलब, कुल मिलाकर लगभग 57% भारतीय ईसाई या तो आदिवासी हैं, या दलित।
UCAN News (2025):
आदिवासी (ST) भारतीय ईसाइयों का हिस्सा लगभग 33% है, और दलित + आदिवासी मिलकर 60% से ज्यादा बनते हैं .
NSSO / अन्य शैक्षणिक रिपोर्ट्स:
कई विद्वानों और कार्यकर्ताओं के अनुसार, दलित ईसाइयों की संख्या 50–75% तक हो सकती है, हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि मुश्किल है .
राज्य-स्तरीय परिदृश्य (आदिवासी समुदायों में ईसाई धर्म का अनुपात)
अरुणाचल प्रदेश:
आदिवासी समूहों में—Wancho 95%, Yobin 99%, Nyishi 63%, Nocte 66%, आदि—अत्यधिक ईसाईकृत (Christian) हैं .
मेघालय:
कुल आबादी में 75% की ईसाई जनसंख्या; Khasi में 83%, Garo में 95% ईसाई धर्मावलंबी हैं .
मणिपुर:
आदिवासी समुदायों में—Thadou, Tangkhul, Poumai आदि—लगभग 97–99% ईसाई हैं .
असम:
लगभग 42.5% ईसाई बहुल आबादी से आदिवासी समुदाय आते हैं .
मिशनरी संगठन और उनका एजेंडा
*”अब बड़ा सवाल—चर्च और मिशनरी संगठन ऐसा क्यों करते हैं?
Joshua Project, जो दुनियाभर में ईसाई मिशन का सबसे बड़ा डेटा-बेस है, खुद लिखता है—
“Followers of Jesus around the world are commissioned to go make disciples of all nations” (Matthew 28:19).
यानी साफ है कि मिशन का लक्ष्य हर राष्ट्र, हर समुदाय को ईसाई धर्म में लाना है।
भारत में भी कई बड़े संगठन इसी मिशन पर काम कर रहे हैं।
Roman Catholic Church (सबसे बड़ा नेटवर्क),
Church of North India (CNI) और Church of South India (CSI),
Evangelical Fellowship of India,
और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर World Evangelical Alliance, Southern Baptist Convention, तथा Jesuit Missions जैसी संस्थाएँ।
ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और समाजसेवा के कामों से जुड़े हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये संस्थाएँ अप्रत्यक्ष रूप से विश्वास निर्माण की प्रक्रिया भी चलाती हैं – जैसे प्रार्थना सभा, चंगाई सभा (faith healing), और गवाही (testimonies) के ज़रिए।
सीधे तौर पर हर स्कूल या अस्पताल को धर्मांतरण का केंद्र कहना गलत होगा। कई जगह ये वास्तव में शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। लेकिन धर्मशास्त्रीय रूप से देखा जाए तो ये संस्थाएँ मिशनरी नेटवर्क का हिस्सा हैं, और इनसे जुड़ी गतिविधियों के पीछे फंडिंग और धार्मिक विस्तार की सोच भी देखी जा सकती है।
स्थानीय अनुभव और सवाल
आदिवासी समाज में अक्सर यह शिकायत सामने आती है कि धर्मांतरण सिर्फ़ आस्था से नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक दबाव, बीमारी से राहत की उम्मीद, या किसी “चमत्कार” की गवाही से भी होता है।
कई बार यह प्रक्रिया इतनी धीमी और अप्रत्यक्ष होती है कि लोग इसे “सहज बदलाव” मान लेते हैं।
लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि “चमत्कार” या “चंगाई सभा” के नाम पर एक तरह का मानसिक प्रभाव डाला जाता है, जिससे लोग पारंपरिक धर्म छोड़कर नया धर्म अपनाते हैं।
“कुछ अध्ययनों में दर्ज है कि शुरुआती दौर में डायन-शिकार जैसी घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से परिभाषित किया गया, और ‘यीशु को न मानने वाले’ लोगों को शैतान-पूजक कहा जाता था। आलोचकों का मानना है कि इसने धर्मांतरण को वैध ठहराने का माहौल बनाया।”
इतिहास और रणनीति
विशेषज्ञों का मानना है कि *”ईसाई मिशनरी भारत में पहली सदी ईस्वी से ही पहुँच चुके थे (सेंट थॉमस के आने की परंपरा मानी जाती है), लेकिन तब उनका प्रभाव सीमित था और ज़्यादातर समुद्री तटीय क्षेत्रों (केरल, तमिलनाडु) तक ही रहा। असली और संगठित मिशनरी गतिविधियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ी सत्ता के आने के बाद शुरू हुईं। उन्होंने समझा कि सीधे ऊँची जातियों या स्थापित धर्मों को बदलना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने निशाना बनाया—आदिवासी और दलित समाज को। क्योंकि ये समाज आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर थे, और साथ ही अपनी परंपरागत आस्थाओं को लेकर किसी संस्थागत सुरक्षा में नहीं थे।
मिशनरियों ने पहले स्कूल खोले, फिर हॉस्पिटल, फिर बाइबल ट्रांसलेशन, और धीरे-धीरे विश्वास बदलने की कोशिश। आज भी यही पैटर्न है—”Service First, Conversion Later”.*
चर्च का जंजाल: आदिवासी दावा बनाम हकीकत
*”जब आप किसी ईसाई बने आदिवासी से बात करेंगे तो वे कहेंगे—‘चर्च धर्मांतरण नहीं कराता, यह हमारी अपनी पसंद थी।’ लेकिन असलियत यह है कि यह ‘पसंद’ एक बहुत लम्बी सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम है। गरीबी में फंसे परिवार को अगर शिक्षा, हॉस्पिटल, नौकरी और पहचान केवल ईसाई धर्म से मिलने लगे, तो धीरे-धीरे पूरा समाज उसी दिशा में खिंच जाता है।
यही कारण है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर-पूर्व भारत और यहां तक कि अंडमान निकोबार तक— आदिवासी इलाकों में चर्च का प्रभाव तेज़ी से बढ़ा है।”*
और सवाल
*”तो क्या यह केवल ‘धर्म की आज़ादी’ का मामला है, या फिर एक सुनियोजित ‘संस्कृतिकरण’ की प्रक्रिया? क्या आने वाले दशकों में सरना, डोनी-पोलो, नियमत्रे, कोया पुनेम, सनामाही और अन्य परंपराएं केवल किताबों और म्यूज़ियम तक सिमट जाएंगी? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या हम एक पूरी सभ्यता खो देंगे?
सोचिए… यह सिर्फ धर्म का सवाल नहीं, बल्कि आदिवासी पहचान, सांस्कृतिक धरोहर और भारत की विविधता के अस्तित्व का सवाल है।*